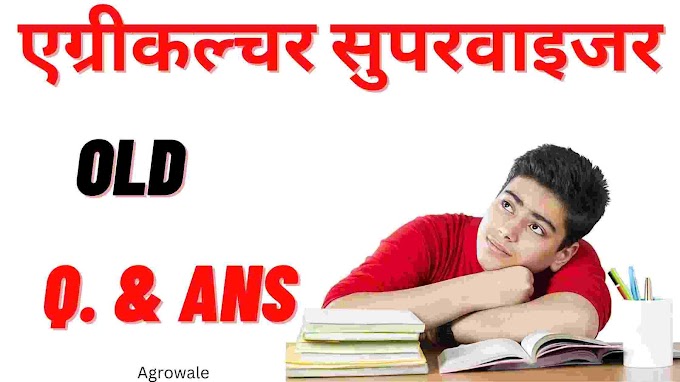IRRIGATION - Irrigation meaning in Hindi
नमस्कार दोस्तों,
स्वागत है आपका हमारे इस आर्टिकल irrigation में, तो दोस्तों आज हमारे इस आर्टिकल मैं irrigation से संबंधित आपके सभी प्रकार के डाउट क्लियर हो जायेंगे। हम इस आर्टिकल मैं सिंचाई से संबंधित मुख्य टॉपिक जैसे– Irrigation meaning in Hindi, Definition of irrigation (सिंचाई की परिभाषा),सिंचाई के उद्देश्य (objectives of irrigation),सिंचाई के लिए फसलों की क्रान्तिक अवस्थाएं,विभिन्न फसलों की जल मांग,सिंचाई की विधियां (methods of irrigation),सींचाई के स्रोत (Source of irrigation) आदि टॉपिक्स का विस्तार पूर्वक विवरण प्रस्तुत किया है। तो आइए आपको लेकर चलते है सीधे हमारे आर्टिकल मैं —
Irrigation meaning in Hindi - Irrigation in Hindi
irrigation meaning in hindi मे बात करे तो इसका मतलब होता
→ सिंचाई करना या पौधों को पानी देना।
Definition of irrigation - सिंचाई की परिभाषा
definition of irrigation सिंचाई की परिभाषा जिसमे हम आपको सम्पूर्ण जानकारी देने वाले है
→पौधों की वृद्धि के लिए मृदा में आवश्यक नमी संभरण हेतु कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं।
अथवा,
→ फासलों को ऊगाने के लिए कृत्रिम रूप से दिया गया जल सिंचन कहलाता हैं।
अथवा,
→वर्षा के अभाव में भूमि को कृत्रिम तरीकों से जल पिलाने की क्रिया को सिंचाई करना कहा जाता है।
★सिंचाई के उद्देश्य (objectives of irrigation):—
(1) पौध वृद्धि हेतु मर्दा में आवश्यक नमी की पूर्ति हेतु।
(2) फसल को अल्पावधि सूखे से बचाकर उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु।
(3) पौध वृद्धि हेतु फसल छत्र (crop canopy) के ऊपर अल्प वायुमंडल (micro atmosphere) को ठंडा रख कर उसे पौध वृद्धि के लिए अनुकूल बनाने हेतु।
(4) कृषण परत (plough layer) को नरम कर उसे कर्षण क्रियाओं हेतु अनुकूल बनाने हेतु।
(5) मर्दा में स्थित लवणों के निक्षालण (leaching) करने या उसे तनू (Dilute) करने हेतु।
(6) फसलों को पाले (frost) से बचाने हेतु।
★सिंचाई के लिए फसलों की क्रान्तिक अवस्थाएं:—
1 गेंहू→शीर्ष जड़ निकलना (Crown root initiation) कल्ले फूटान (Late tillering), गाँठ अवस्था (Late jointing), बालिया निर्माण (Ear emergence), दाने की दूधिया अवस्था (Milk stage) व दाना पकने की अवस्था (Dough stage)
2. जौ→ बुवाई के 30 दिन बाद, दाने भरते समय
3. चना,सरसों,अलसी→ फूल आने से पहले, फलियां बनते समय
4. आलू→ अंकुरण के समय,कन्द बनने का प्रारम्भिक समय
5. गन्ना→ फॉर्मेटिव अवस्था (जड़ो की वृद्धि), अंकुरण, कल्ले निकलते समय, बढ़वार के समय
6. कपास→ डोडे वाली शाखायें (सिंपोड) बनते समय, फूल आते समय, डोडे बनते समय
7. तम्बाकू→ चुटाई के समय
8. मूँगफली→ सुइयाँ बनने से मूँगफली बनना शुरू होने तक
9. धान→ कल्ले निकलते समय, फूल आने से पहले व फूल आते समय
10. मक्का→ नरमंझरी आते समय, भुट्टे बनते समय ( बूटिंग अवस्था)
★विभिन्न फसलों की जल मांग:—
फसल≈ जल मांग (mm)
1. गन्ना→ 1500-2500
2. धान → 900-2500
3. कपास → 700-1300
4. मक्का→ 500-800
5. आलू → 500-700
6. मुंगफली → 500-700
7. सोयाबीन → 500-700
8. गेंहू → 450-650
तो साथियों समझ गए होंगे की definition of irrigation सिंचाई की परिभाषा क्या है
सिंचाई की विधि methods of irrigation in hindi
सिचाई की विधि (irrigation methods) के कुछ प्रकार इस प्रकार है
[1.] चौकेबार द्रोणी सिंचाई विधि —
खेतों में सिंचाई हेतु यह सर्वाधिक प्रचलित विधि है। इस विधि के अंतर्गत खेत का समतलीकरण कर उसे वर्गाकार अथवा आयताकार क्यारियों में विभाजित कर दिया जाता है। इन क्यारियों को चौकेबार(check basin) कहती है। खेत में ढाल अनुसार क्यारियों में जल प्रवाह हेतु नालियां बनाई जाती है। प्रत्येक चौकेबार में आवश्यकता अनुसार पानी भरा जाता है।
#लाभ →
1. समतल भूमि का अनियंत्रित आप्लावन विधि की अपेक्षा अधिक जल सदुपयोग दक्षता प्राप्त की जाती है।
2. अपवाह व अंत: स्त्रावण जैसी समस्या में कमी आती है।
3. खेत में जल वितरण समान होता है।
4. सरल विधि है।
#समस्याऐं →
1. खेत में पानी परवाह है हेतु बनाई गई नालियों में भूमि का बड़ा भाग बुवाई के काम में नहीं आता है।
2. नालियों से खेत में मशीनों के उपयोग में कठिनाई व निराई गुड़ाई में व्यवधान उत्पन्न होता है।
3. पृष्ठीय जल निकास बाधित होता है।
4. खेत में अपेक्षाकृत समतलीकरण होना आवश्यक होता है।
5. खेत की तैयारी में अधिक मजदूर चाहिए।
[2.] बोर्डर पट्टी सिंचाई विधि (Border strip irrigation method):—
इस विधि में खेत के ढाल की दिशा में लंबी लंबी पटिया समानांतर रूप से बनाई जाती है प्रत्येक पट्टी में ऊपर की ओर से पानी छोड़ा जाता है जोकि महीन परत के रूप में निचले सिरे की ओर बहता हुआ आता है प्रत्येक पट्टी की लंबाई व चौड़ाई जल बहाव, ढलान प्रतिशत व भूमि की बनावट के अनुसार होती है यह विधि पास पास बोई जाने वाली फसल जैसे– गेहूं इत्यादि के लिए उपयुक्त है।
#लाभ→
1.आसान विधि है।
2.अधिक जल मात्रा व प्रवाह को आसानी से प्रयुक्त किया जा सकता है।
3. निराई गुड़ाई व मशीन के प्रयोग में सुगमता होती है।
4. मेड़ों व नालियों के रखरखाव में कम खर्च होता है।
5. जल निकास की व्यवस्था करना आसान होता है।
#समस्याएं→
1. ऊबड़–खाबड़ स्थलाकृति की भूमि में यह विधि अपनाना संभव नहीं है।
2. धान जैसी फसलों में इस विधि से सिचाई करना संभव नहीं है।
3. यदि जल प्रवाह है वह मात्रा कम हो तो इस विधि से सिचाई संभव नहीं है।
4. बॉर्डर की संपूर्ण चौड़ाई में एक समान जल प्रवाह कठिन होता है।
[3] कुण्ड सिंचाई विधि:—
यह विधि पंक्तियों में बोई जाने वाली फसलों जैसे मक्का, ज्वार इत्यादि के लिए उपयोगी होती है अधिक ढाल वाले क्षेत्रों में ढाल की आड़ी दिशा में समोच्च रेखा पर बनाए जाते है।
♠ लाभ:→
1. वाष्पन द्वारा जल हास्य व पपड़ी बनाने की समस्या नहीं होती है।
2. कम मजदूरों की आवश्यकता होती है।
3. चौकेबार विधि की अपेक्षा खेत का कम भाग मेड व नालियों में काम आता है।
♠ समस्याएं:→
1. अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा अपरदन की संभावना रहती है।
2. मेड़ों पर लवण एकत्रित होकर पौध वृद्धि पर विपरीत प्रभाव डालते हैं।
3. बलुई मर्दा हेतु उपयुक्त नहीं है।
4. पानी के दक्ष नियंत्रण हेतु कुशल मजदूर चाहिए।
[4.] अवपृष्ठिय या अधोभूमि सिंचाई (sub–Surface irrigation):—
कुछ स्थानों पर भूमि व स्थलाकृति की प्राकृतिक परिस्थितियां पौधों की जड़ों में जल की प्रयुक्त भूमि की सतह के नीचे से करने के लिए अनुकूल होती है इसमें धरातल के नीचे पर एक निश्चित गहराई पर कृत्रिम जल स्तर बनाए रखकर फसल को जलापूर्ति की जाती है जल खुली नालियों या रंद्र युक्त पाइप द्वारा की जाती है।
[5.] बौछारी सिंचाई विधि (Sprinkler irrigation method) :—
इस विधि में पानी को बौछार अथवा वर्षा के रूप में वितरित किया जाता है यह सिंचाई प्रणाली में पंप द्वारा मुख्य व शाखा पाइप लाइनों में जल पहुंचाया जाता है जहां से वह राइजर(Riser) के ऊपरी सिरे पर लगे घूर्णी बौछार यंत्र(Rotating sprinkler head) द्वारा फुहार के रूप में फसल के ऊपर गिरता है।
♦ लाभ:→
1. बौछारी प्रणाली पृष्ठिय विधि की अपेक्षा सुगम व सरल है।
2. समस्त जमीन फसल उगाने के काम आती है जबकि पृष्ठिय भूमि का कुछ भाग मेड बनाने में काम आता है।
3. मेड़ न होने से यंत्रीकरण संभव है।
4. हल्की व ब्लूई मृदा में जहां बार-बार पानी देना पड़ता है बौछारी विधि अधिक उपयोगी है।
5. चूंकि खेत पर पानी पाइपों से पहुंचता है अतः रास्ते के जल हास्य(Conveyance loss) नहीं होता है।
6. मर्दा पर पपड़ी बनने की समस्या नहीं होती है।
7. फसल का पाले से स्वत: बचाव हो जाता है।
8. सिंचाई के साथ ऊर्वक भी दिया जा सकता है।
9. यह विधि पौधों को वातावरण में आद्रता बनाए रखने में सहायक होती है।
♦ समस्याएं:→
1. अधिक जल मांग वाली फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है।
2. छोटे खेतों में अधिक लागत बैठती है।
3. अधिक वायु गति होने पर जल वितरण असमान होकर दक्षता घटती है।
4. पानी साफ नहीं होने की स्थिति में घूर्णी बौछार यंत्र अवरुद्ध हो सकते है।
5. लवणीय जल हेतु उपयुक्त विधि नहीं है।
6. आरंभिक खर्च अधिक है।
7. पर्याप्त तकनीकी ज्ञान आवश्यक है।
[6.] बूंद– बूंद सिंचाई विधि (Drip irrigation system):—
इस विधि का अविष्कार इजराइल से हुआ यह विधि शुष्क व अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों में जहां वर्षा कम होती है मिट्टी बलुई है वह वाष्पन– वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल हानी अधिक होता है अत्यंत उपयोगी है ड्रिप सिंचाई द्वारा जल प्रत्येक पौधे की जड़ के पास बूंद-बूंद टपकता है इसमें जड़ क्षेत्र में संतृप्तअवस्था बनी रहती है तथा वहां पानी की कमी नहीं रहती है इस विधि द्वारा उड़ानों, सब्जियों, पंक्तियों में बोई जाने वाली फसलों जैसे गन्ना, कपास इत्यादि में सिंचाई की जाती है।सिचाई की विधि (irrigation methods)
♣ लाभ:→
1. पौधों की जड़ों में पर्याप्त नमी होने से अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है।
2. पौधों के बीच सुखा रहने से खरपतवार की समस्या नहीं होती हैं।
3. सिंचाई के साथ-साथ एक ही बार में उर्वरक भी दिया जा सकता है।
4. सिंचाई हेतु कम मानव श्रम चाहिए।
5. कीट– व्याधि की समस्या कम होती है क्योंकि पौधों के पास का वातावरण आध्र नहीं होता है।
6. बार-बार सिंचाई करने से लवणों का निक्षालन हो जाता है।
7. कम पानी की आवश्यकता होती है।
8. जल उपयोग दक्षता अधिक होती है।
♣समस्याएं:→
1. प्रारंभिक व्यय अधिक होता है।
2. कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है।
3. उत्सर्जक (Emitter) का छिद्र छोटा होने से मिट्टी के कणों, जीवांश पदार्थ के रेशे, लवण के कणों से बंद हो सकते हैं।
4. अत्यधिक भारी मर्दा की अंतर स्पंदन दर कम होने से जल एकत्रित होने की समस्या हो सकती है।
5. प्लास्टिक से बनी पार्श्व नलिकाएं चूहे व अन्य कीट नष्ट कर सकते हैं।
6. वार्षिक फसलों में बार-बार लगाना वह हटाना पड़ता है।
तो कैसा लगा सिचाई की विधि (irrigation methods) जो हमने सम्पूर्ण तरीके समझने का प्रयास किया है
सींचाई के स्रोत - Source of irrigation in hindi
सिंचाई के स्त्रोत (Source of irrigation) वह स्थान है जहां पर जल एकत्रित रहता है जिन्हें जल भंडार भी कहते हैं जैसे– कुआं नैहरे, तालाब, बावड़ी, झील, झरने, सीवर, नदियां आदि।
सींचाई के मुख्य स्त्रोत(Source of irrigation) निम्नलिखित हैं:
{1} नहरें (Canals):→ नदियों पर बांध बनाकर नेहरें निकाली जाती है फिर इनके जल का सिंचाई हेतु उपयोग किया जाता है बांध तथा नहरों के निर्माण में काफी पूंजी तथा समय की आवश्यकता होती है।
♠ नहरों के प्रकार—
(A) अनित्यवाही नहरें(Seasonal canals) ≈
इन्हे बरसाती नहरें भी कहते हैं। नदियों के जल की बाढ़ को कम करने के लिए अथवा रोकने के लिए यह नेहरे बनाई जाती है जिनका पानी सिंचाई के काम आता है नदियों में जलस्तर एक निश्चित ऊंचाई से ऊपर जाने लगता है तो पानी को इन नहरों में छोड़ दिया जाता है इन नहरों के मुख्य रूप से दो दोष है प्रथम जब नदी में पानी नीचे रह जाता है तो इन नहरों में पानी नहीं जाता और नेहरे सूख जाती है दूसरा इन नहरों से पूरे वर्ष सिंचाई नहीं होती। अतः इन नहरों का बनवाना अधिक लाभदायक नहीं रहता इसलिए अब इस प्रकार की नहरें कम बनवाई जाती है इस प्रकार की नहरों के उदाहरण भारत में कृष्णा, कावेरी, डेल्टा क्षेत्रों में है।
(B) नित्यवाही नहरें ≈
इन्हें बारहमासी नैहरे भी कहते हैं क्योंकि इनमें पूरे वर्ष पानी बहता रहता है और यह पूरे वर्ष सिंचाई के काम आती है यह नैहरे हमेशा बहने वाली नदियों से निकाली जाती है अथवा नदियों पर बांध बनाकर निकाली जाती है उदाहरण इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, बूंदी आदि जिलों में नहर सिंचाई का मुख्य स्त्रोत है बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा बनाई गई गंग नहर राजस्थान की ही नहीं देश की भी प्राचीनतम नहर प्रणालियों में से एक है जिससे वर्तमान में भी सिंचाई की जा रही है।
{2} तालाब (Tanks):→
तालाब किसी का व्यक्तिगत नहीं होता है प्राय: एक गांव का एक तालाब होता है जो गांव के निचले भाग में स्वत: बन जाता है इसमें पूरे गांव एवं आसपास से वर्षा का पानी आकर एकत्रित होता है जहां धरातल कुएं खोदने के लायक नहीं है इस कारण तालाब की आवश्यकता होती है राजस्थान में भीलवाड़ा, टोंक आदि क्षेत्रों में तालाब सिंचाई के अच्छे स्रोत हैं।
{3} कुएँ (Wells) :→
कुओं के माध्यम से सिंचाई परंपरागत रूप से की जाती रही है कुआं द्वारा सिंचाई में अधिक व्यय एवं परिश्रम की आवश्यकता होती है राजस्थान में सिंचाई का सबसे प्रमुख स्रोत कुएं हैं।
♠ कुओं के प्रकार—
1. अस्थाई कुंआ
2. स्थाई कुआं – ये दो प्रकार के होते है
(a) कच्चा कुंआ
(b) पक्का कुंआ
3. पाताल तोड़ कुंआ ( Artisan Wells)
4. नलकुप्त(Tubewell)
5. झीलें
6. झरने (Cascade)
7. बावड़ियां
तो अब आप समझ गए होंगे की सिंचाई के स्त्रोत (Source of irrigation) के प्रकार क्या है
तो दोस्तों आपने आर्टिकल पढ़ लिया है मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आर्टिकल पसंद आया होगा, क्योंकि हमने इस आर्टिकल मैं पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। फिर भी अगर हम से कोई टॉपिक छूट गया ह तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूं कि आपके सिंचाई irrigation से संबंधित सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। जिसमे हमने (Irrigation meaning in Hindi, irrigation types और irrigation methods पर चर्चा की है ।
अगर आपको हमारा आर्टिकल पढ़कर अच्छा लगा है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इसी ही जानकारी निरंतर पाने के लिए हमसे जुड़ें रहें। और कोई भी सवाल हो तो कॉमेंट करके जरूर पूछना
धन्यवाद।
Team— agrowale